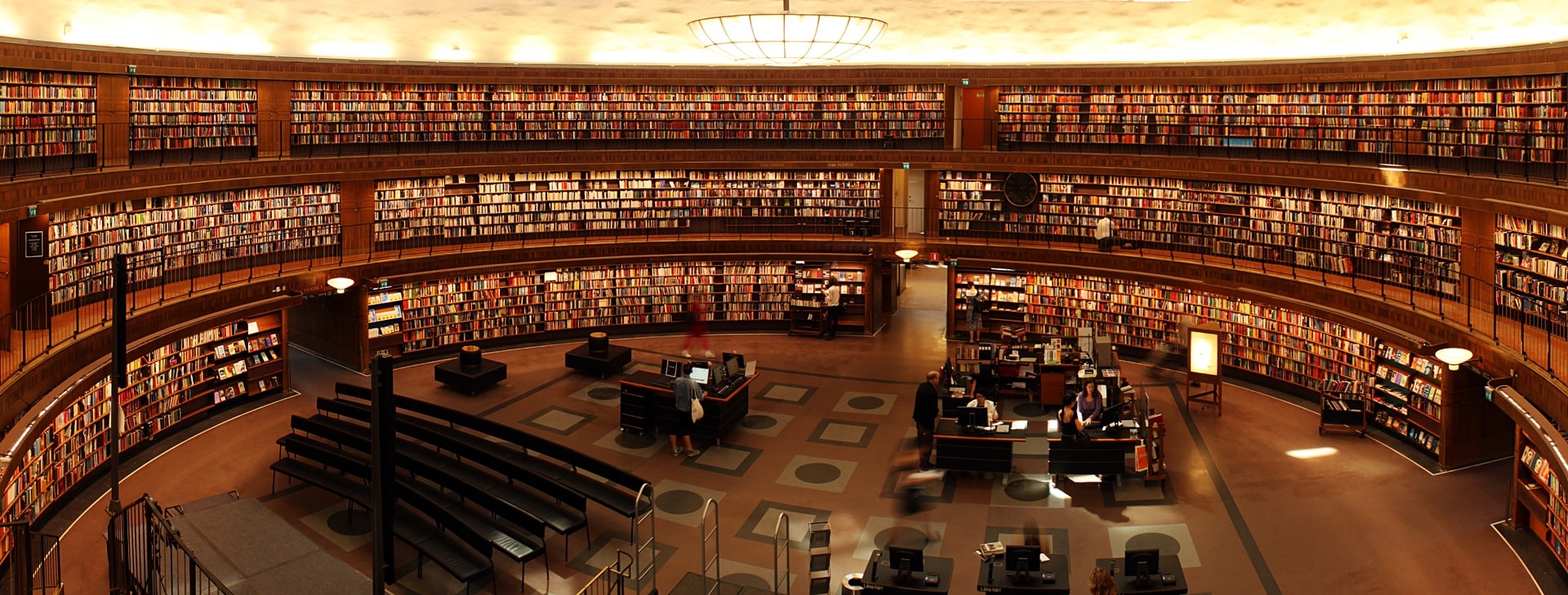व्यापारिक सन्नियम (Business / Mercantile Law) व्यवसाय के संचालन, नियंत्रण तथा अन्य कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे आप आज के इस पोस्ट में पढ़ने वाले हैं। इस आर्टिकल में आप व्यापारिक सन्नियम का इतिहास, क्षेत्र (विषय-वस्तु) भारत में व्यापारिक सन्नियम तथा स्त्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेगें।
व्यापारिक सन्नियम का इतिहास
Business Law व्यापार रूढ़ी की देन हैं। इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी से पहले व्यापार रूढ़ी उन नियमों का संग्रह माना जाता था जो कि common-law से बिल्कुल अलग थे। व्यापारियों के पारस्परिक व्यवहार इन्हीं रूढ़ियों के द्वारा प्रशासित होते थे। उनके विवादों का निर्णय मेलों और मंडियों में एकत्रित व्यापारियों में से कुछ विशेष व्यक्तियों के समक्ष अथवा उन्हीं के पृथक् न्यायालयों द्वारा किया जाता था जो कि Courts of Piepondrous के नाम से प्रसिद्ध थे।
17 वीं शताब्दी तक उपर्युक्त प्रकार के न्यायालय पूर्ण रूप से लुप्त हो चुके थे किंतु उनके द्वारा विकसित रीति-रिवाजों को Common Law ने ग्रहण कर लिया एवं उनका विकास किया गया हैं।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड में वास्तविक रुप से व्यापार सन्नियम का विकास हुआ । यह रीति रिवाज आज भी इंग्लैंड के व्यापारिक सन्नियम का एक प्रमुख अंग माना जाता हैं।
व्यापारिक सन्नियम का क्षेत्र (विषय-वस्तु)
सच में देखा जाए तो व्यापारिक सन्नियम का क्षेत्र अधिक व्यापक है क्योंकि यह सन्नियम केवल व्यापारियों एवं उद्योगपतियों पर ही लागू नहीं होता बल्कि समाज के सभी लोगों पर लागू होता हैं।जैसे कि –
- वस्तु विक्रय अधिनियम
- साझेदारी अधिनियम
- अनुबंध अधिनियम
- बीमा अधिनियम
- पेटेंट, ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट अधिनियम
- विनिमय साध्य विलेख अधिनियम
- दिवालिया अधिनियम
- आवश्यक वस्तु अधिनियम
- एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहारअधिनियम कंपनी अधिनियम।
भारत में व्यापारिक सन्नियम
सन् 1872 से पहले भारत में व्यापारिक लेन-देन पक्षकारों से संबंधित कानून से नियंत्रित होते थे । जैसे हिंदू Law मुस्लिम Law । सन् 1872 में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 बनाते समय प्रथम बार यह प्रयास किया गया था कि भारतीय व्यापारिक सन्नियम के एकरूपता वाले सिद्धांतों को स्थापित किया जाए।
भारतीय व्यापारिक सन्नियम अधिकांश इंग्लैंड के व्यापारिक सन्नियम पर ही आधारित है।
” भारतीय व्यापारिक सन्नियम मुख्यतः इंग्लैंड के व्यापारिक सन्नियम की ही एक नकल हैं। “- बी.एन. राय
Read More –मांग के नियम से आप क्या समझते हैं?
भारतीय व्यापारिक सन्नियम का स्तोत्र क्या है?
वास्तव में देखा जाए तो भारतीय व्यापारी सन्नियम इंग्लैंड के व्यापारिक सन्नियम पर ही आधारित है इसका कारण यह है कि भारतीय व्यापारिक सन्नियमों से संबंधित अधिकतर अधिनियम अंग्रेजी शासनकाल में ही बनाए गए हैं । कहीं-कहीं स्थानीय एवं रूढ़ियों के आधार पर इन में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं।
विद्वानों के अनुसार भारतीय व्यापारिक सन्नियम के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं जो नीचे इस प्रकार से दिए गए हैं-
- आधारभूत न्यायिक निर्णय (Leading and Judicial Decisions)
- अंग्रेजी कॉमन लॉ (English Common law)
- परिनियम अथवा संसद द्वारा निर्माण किए गए सन्नियम
- साम्य एवं न्याय-सिद्धांत (Principles of Equity and Justice)
अंग्रेजी कॉमन लॉ (English Common law)
इंग्लैंड का कॉमन लॉ नियमों का वह समूह है जिसका कि प्रमुख स्रोत सामान्य रूढ़िवादी प्रथाएं एवं रीती रिवाज थीं। भारत में लेखबद्ध अधिनियमों की अपर्याप्तता के कारण हमको विवश होकर अंग्रेजी कॉमन लॉ का सहारा लेना पड़ता हैं। यदि किसी मामले में भारतीय व्यापारिक सन्नियम के प्रावधान अपर्याप्त हो तो हमें अंग्रेजी सन्नियम का ही सहारा लेना पड़ता है।
आधारभूत न्यायिक निर्णय (Leading and Judicial Decisions)
उपर्युक्त महत्वपूर्ण स्रोत एवं सिद्धांतों के अलावा भारतीय न्यायालय प्रायः हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आधारभूत निर्णय का भी सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष , लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त आदि के विवाद।
परिनियम अथवा संसद द्वारा निर्माण किए गए सन्नियम
वे सन्नियम जो कि किसी देश की संसद अथवा विधान सभा द्वारा निर्माण किए गए होते हैं परिनियम अथवा संसद द्वारा निर्मित परिनियम कहलाते हैं। भारतीय व्यापारिक सन्नियम के निर्माण में भारतीय संसद एवं विधान सभाओं का महत्वपूर्ण हाथ रहा है।
जैसे वस्तु विक्रय अधिनियम , साझेदारी अधिनियम एवं कंपनी अधिनियम, आदि।
साम्य एवं न्याय-सिद्धांत (Principles of Equity and Justice)
प्राचीन काल में अन्य देशों की भांति इंग्लैंड में राजा जनता की शिकायतों को सुनते और उसका समाधान करते । कुछ समय पश्चात राजा इन शिकायतों को अपने चांसलर को प्रेषित करने लगे । चांसलर जो कि पादरी होता था। इन शिकायतों का निपटारा कानून के कठोर नियमों के अनुसार ना करके प्राकृतिक न्याय,सामान्य विवेक एवं समाजिक उचित सिद्धांतों के अनुसार किया करता था।
चांसलर द्वारा इस प्रकार जिन सिद्धांतों का मिश्रण होता था वही साम्य सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ।