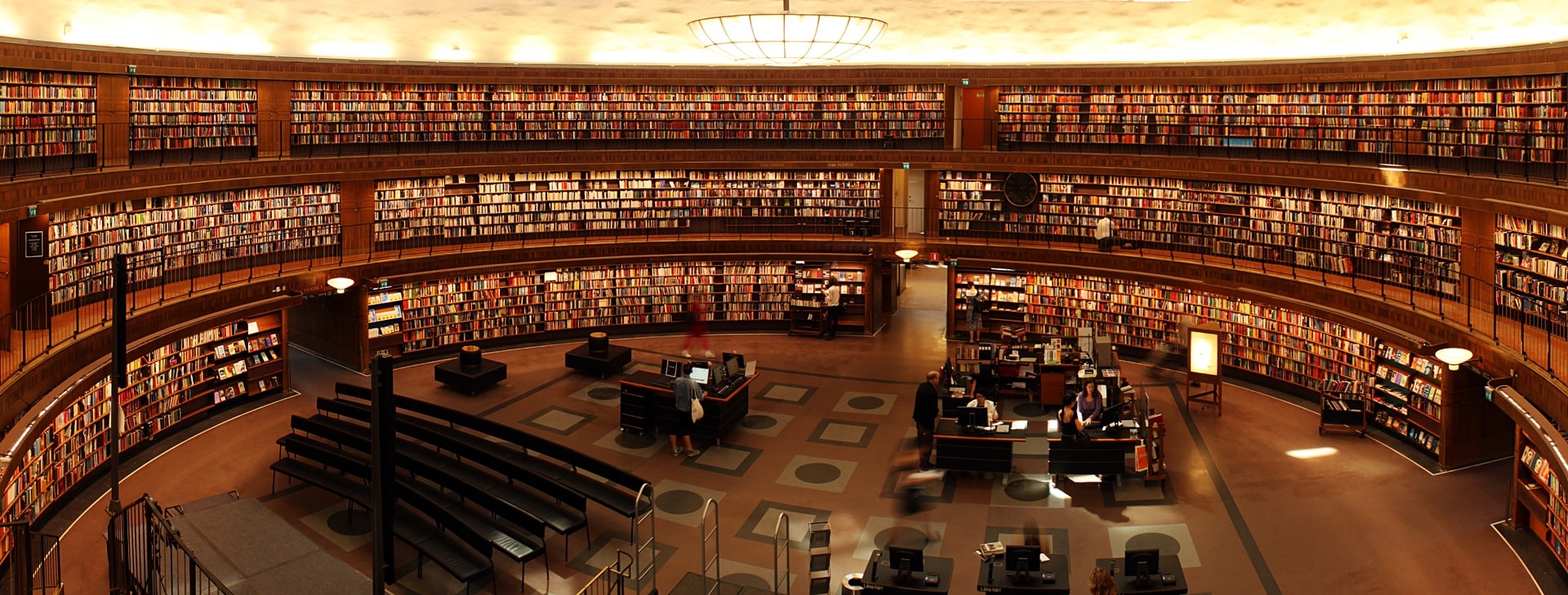हेलो स्टूडेंट, आज के इस नए आर्टिकल में आप लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पढ़ेगे। जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है।
लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करें
लेखांकन सिद्धांतों में लेखांकन की अवधारणा को शामिल किया गया है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा के कुछ सिद्धांत अथवा नियम होते हैं जो कि उसकी समस्याओं को सुलझाने में निर्देशक का कार्य करते हैं। मानव अपने उद्देश्य की पूर्ति, उपयोगिता और अपने साधनों व व्यवसाय के आकार-प्रकार के अनुरूप विभिन्न सिद्धांतों को अपना सकता हैं।
लेखा विधि के सिद्धांत विश्वव्यापी नहीं है। यह एक देश से दूसरे देश में, एक नगर से दूसरे नगर में, एक गांव से दूसरे गांव में तथा एक व्यापार से दूसरे व्यापार में अलग-अलग पाए जाते हैं। लेखा विधि के सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत नहीं है यह तो अवधारणाएं हैं।
जो अपने सुविधा उपयोगिता व उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार अपनाया जा सकते हैं। व्यवसायी अपनी सुविधा एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्तपालन Book-Keeping करता है अन्यथा उसे कानून बाध्य नहीं करता। यद्यपि संयुक्त स्कंध कंपनियों व विशिष्ट संस्थाओं को वैधानिक तौर पर निर्धारित लेखा विधि अपनानी पड़ती हैं।
कुछ विद्वान लेखांकन की अवधारणा तथा प्रथाओं दोनों को ही लेखांकन सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल कर देते हैं इस आधार पर लेखांकन के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं।
- मुद्रा मापन का सिद्धांत
- व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत
- व्यवसाय के चालू स्थिति का सिद्धांत
- लागत का सिद्धांत
- दोहरा पहलू की अवधारणा का सिद्धांत
- रूढ़िवादिता का सिद्धांत
- वसूली का सिद्धांत
- अनुरूपता का सिद्धांत
- एकरूपता का सिद्धांत
- सारता का सिद्धांत
#1 मुद्रा मापन का सिद्धांत
लेखांकन में केवल उन्हीं लेन- देनों तथा घटनाओं का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा Money के रूप में व्यक्त किया जा सके अर्थात लेखा पुस्तकों में वैसे ही व्यापारिक लेन-देन एवं तत्व को लिखे जाते हैं जिनकी मुद्रा में माप करना संभव हो। इस सिद्धांत ने लेखांकन के क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया है क्योंकि किसी ऐसी घटना का लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करना संभव नहीं है जिसे मुद्रा में नहीं मापा जा सकता हो।
जैसे लेखांकन में – व्यवसाय स्वामी के स्वास्थ्य, प्रबंधकों की योग्यता, प्रतियोगिता में वृद्धि आदि का लेखा नहीं किया जाता है जबकि यह व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके कारण लेखांकन व्यवसाय की स्थिति का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत नहीं हो पाता है।
#2 व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत
लेखांकन में व्यवसाय को व्यवसाय से पृथक एक स्वतंत्र इकाई समझा जाता है और व्यवसाय में किए जाने वाले लेखे व्यवसाय – मालिक या किसी अन्य संबंधित पक्ष की दृष्टि से न किए जाकर व्यवसाय की दृष्टि से किए जाते हैं। किसी व्यवहार का व्यवसाय की पुस्तकों में लेखा करते समय लेखापाल यह देखता है कि उस व्यवहार का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, न कि व्यवसाय के मालिक, प्रबंधक या व्यवसाय के किसी अन्य संबंधित पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
यह सिद्धांत लेखांकन के ढांचे के लिए आवश्यक है। यदि व्यवसाय को व्यवसाय – मालिक, मैनेजर, लेनदार या अन्य संबंधित पक्षों से पृथक ना रखा गया तो लेखे व्यवसाय की सही चित्र प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं इसके अलावा लेखांकन की अन्य सिद्धांत भी इस सिद्धांत से प्रभावित होती हैं। व्यवसाय के स्वतंत्र अस्तित्व के कारण ही व्यवसाय को अनिश्चित लंबे समय तक चलते रहने की संभावना बनी रहती हैं।
#3 व्यवसाय के चालू स्थिति का सिद्धांत
जब तक इसके विरूद्ध कोई प्रमाण न हो तब तक यह माना जाता है कि व्यवसाय भविष्य में अनंत काल तक चलता रहेगा। इस मान्यता का यह महत्व इसके संभावित विकल्पों की तुलना करने पर प्रकट होता है। इस स्थिति में कोई भी व्यवसाय संस्था ना तो कोई संविदात्मक वादे Contractual Commitment कर सकेगी और ना ही अपने साधनों को पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर प्रयोग कर सकेगी। इस दशा में लेखांकन में सदैव यह प्रयास रहेगा कि पुस्तकों में व्यवसाय के क्रेता की दृष्टि से मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य दिखलाया जाए लेकिन बिजनेस की चालू स्थिति की अवधारणा के अंतर्गत ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती और वास्तव में व्यवहार में ऐसा नहीं किया जा सकता।
लेखांकन में इनका वर्तमान मूल्य निरर्थक होता है क्योंकि इन्हें बाजार में ना तो बेचा जा सकता है और ना ही व्यवसाय में भविष्य उत्पादन के लिए प्रयोग ही किया जाता है। इस सिद्धांत के कारण ही स्थायी संपत्तियों पर ह्रास व अन्य लंबे व्ययों को उनके उपयोगी जीवनकाल पर फैलाकर ज्ञात किया जाता है।
#4 लागत का सिद्धांत
यह सिद्धांत व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित लागत की अवधारणा हैं। इस अवधारणा के अनुसार समस्त लेन – देनों को लेखांकन अभिलेखों में उनके प्राप्त करने की मौद्रिक लागत पर दिख लाया जाता हैं, उनके वर्तमान मूल्य या प्रतिस्थापन मूल्य पर नहीं। इसलिए सभी संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर दिखया जाता है, चाहे उनका बाजार मूल्य या प्रतिस्थापन मूल्य लागत मूल्य से भिन्न ही क्यों ना हो तथा ऐसी संपत्तियां या मदें जिनके लिए व्यवसाय को कुछ नहीं देना पड़ता है उन्हें लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जाता हैं।
#5 दोहरा पहलू की अवधारणा का सिद्धांत
यह सिद्धांत व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयोगी होता हैं। इसका अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय की प्रत्येक लेनदेन दो पक्ष पर आधारित होते हैं – डेबिट पक्ष व क्रेडिट पक्ष । इसमें प्रत्येक लेन-देन दोनों समान रूप से प्रभावित होते हैं। तकनीकी भाषा में “For every debit, there is a credit.” इसलिए चिट्ठे के डेबिट व क्रेडिट का योग सदैव एक समान रहता हैं। व्यवसाय में प्रत्येक लेन – देन से व्यवसाय की संपत्ति और उन संपत्तियों के विरुद्ध दूसरे पक्षों के दावों अर्थात समताओं को समान रूप से प्रभावित करता है इसलिए व्यवसाय की संपत्ति और समता सदैव समान होती है।
#6 रूढ़िवादिता का सिद्धांत
‘लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें’। यह इस अवधारणा का सार हैं। इस अवधारणा के अनुसार लेखों में सभी संभावित हानियों पर ध्यान दिया जाता है जबकि सभी संभव लाभों को छोड़ दिया जाता हैं।
एक प्रसिद्ध व्यक्ति के शब्दों में ‘ संदेह की दशा में वह तरीका अपनाया जाएगा जिससे लाभ का अंक अथवा संपत्ति मूल्यांकन न्यूनतम रहे।’ इस तरह जहां कहीं भी लेखापाल के समक्ष उचित चयन की समस्या आती है तो उसका सदैव ही यह प्रयास रहता है कि लेखा-पुस्तकों में व्यवसायिक लेन-देन इस प्रकार रिकॉर्ड किए जाए जिससे स्वामियों की क्षमता कभी भी अधिक ना दिखाई दे।
#7 वसूली का सिद्धांत
आय के निर्धारण में इसका विशेष महत्व होता हैं। यह आगमों के अर्जन के समय-बिंदु के निर्धारण से संबंधित हैं। इस अवधारणा के अनुसार कोई भी आगम उस समय में अर्जित हुआ माना जाता है जब वह विक्रय हो जाए अथवा जब उसकी वसूली निश्चय हो जाए।
उदाहरण के रूप में – विक्रय के प्रसंविदे में आगम तब अर्जित माना जाता है जबकि बेचे गए माल का अधिकार क्रेता को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दिया गया हो और व्यवसाय द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में आगम तब वर्जित माना जाता है जबकि व्यवसाय द्वारा ग्राहक सेवा प्रदान की जा चुकी हैं।
#8 अनुरूपता का सिद्धांत
निर्धारण में इस अवधारणा का भी काफी महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार आय ज्ञात करने के लिए जब आगम और व्यय की तुलना की जाए तो वे अनुरूप होने चाहिए। आगम और व्यय के अनुरूप होने का मतलब यह है कि यह दोनों एक ही लेखाविधि, उत्पादन, इकाइयों, व्यवसायों, विभागों आदि से संबंधित होनी चाहिए।
#9 एकरूपता का सिद्धांत
इसका मतलब यह है कि संस्था में वर्ष प्रति वर्ष एक सी लेखा-विधि पद्धति, विधियों, कार्य-प्रणालियों को अपनाया जाए तथा उनमें बार-बार परिवर्तन ना किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार यह आशा की जाती है कि एक कंपनी ने एक बार जिस पद्धति को अपनाने का निर्णय कर लिया, आगे आने वाले उसी प्रकृति की अन्य घटनाओं के लिए भी वह उसी तरीकों को अपनाती रहेगी।
यह सिद्धांत विशेष रूप से वहां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं जहां वैकल्पिक लेखा- पद्धति भी समान रूप से स्वीकार्य हैं। वित्तीय लेखा-विधि में ऐसे बहुत से क्षेत्र है जहां विभिन्न वैकल्पिक पद्धतियों का प्रयोग संभव है।
#10 सारता का सिद्धांत
सारता का आशय किसी मद या घटना के सापेक्षिक महत्व से होता हैं। प्रत्येक व्यवहार या घटना की आर्थिक उपयोगिता और महत्ता कुछ सीमा तक लेखा-अभिलेखों को प्रभावित करती हैं। इस अवधारणा के कारण लेखा विधि में केवल उन्हीं घटनाओं तथा तथ्यों का उल्लेख किया जाता है जो कि महत्वपूर्ण व उपयोगी है तथा सारहीना घटनाओं व तथ्यों, जिनका वित्तीय निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, की उपेक्षा की जाती हैं।
इसी अवधारणा का पालन करते हुए जब कभी छोटी राशि की मदें आती है तो व्यवहार में बहुधा उन्हें छोड़ दिया जाता है।
निष्कर्ष – लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत में उपयुक्त जो बिंदु दिए गए हैं वह सभी महत्वपूर्ण है। अब आप बहुत ही आसानी से लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत व अवधारणा क्या – क्या होते हैं उसे आप समझ गए होंगे।